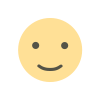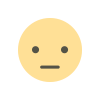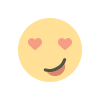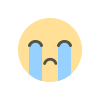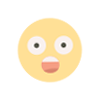Wakf संशोधन पर Supreme Court का आदेश, केंद्र सरकार की आपत्ति

देश में इन दिनों वक्फ संशोधन कानून और पॉकेट वीटो को लेकर जारी राजनीतिक घमासान अब संसद और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बहस तक पहुंच गया है। इस मुद्दे पर सियासत गर्म होती जा रही है और लोकतंत्र के स्तंभों के बीच तालमेल पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "अगर कानून बनाना अब कोर्ट का ही काम रह गया है, तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए।" उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया, जो अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या है वक्फ कानून का मामला?
दरअसल, वक्फ कानून में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश से पहले अपनी बात रखने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि:
-
गैर-मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में एंट्री पर रोक रहेगी
-
‘वक्फ बाय यूजर’ संपत्तियों में किसी भी प्रकार का बदलाव फिलहाल नहीं किया जाएगा
इस आदेश के बाद सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने इसे न्यायपालिका का विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करार दिया।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "न्यायपालिका को विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दोनों संस्थाओं को एक-दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करना जरूरी है।"
वक्फ जेपीसी के पूर्व अध्यक्ष का बड़ा दावा
जगदंबिका पाल, जो वक्फ से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं, ने इस मसले पर और भी आगे बढ़ते हुए कहा, "अगर यह साबित हो गया कि कानून में कोई गलती है, तो मैं सांसद पद से इस्तीफा दे दूंगा।"
पॉकेट वीटो पर भी सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा वर्षों से लंबित 10 विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, अन्यथा यह संविधान के खिलाफ माना जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस आदेश को कार्यपालिका की संवैधानिक भूमिका में कटौती बताते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि इस तरह की समय-सीमा तय करने से शासन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
क्या लोकतंत्र में शक्ति-संतुलन पर पुनर्विचार जरूरी?
अब बड़ा सवाल यही है कि जब न्यायपालिका विधायिका की सीमाओं की समीक्षा कर रही है और विधायिका खुद को कमजोर महसूस कर रही है — तो क्या यह समय आ गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे में शक्तियों के संतुलन को नए सिरे से परिभाषित किया जाए?
यह बहस आने वाले दिनों में और भी गहराने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक कानून या आदेश का मामला नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक संतुलन से जुड़ा अहम मुद्दा बनता जा रहा है।